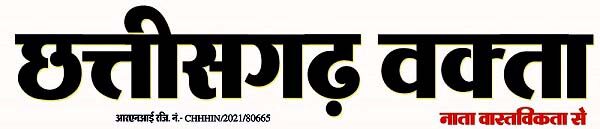- डॉ. बेठियार सिंह साहू
सहायक प्राध्यापक, हिन्दी
हिन्दी, प्रयोक्ताओं की संख्या और भौगोलिक विस्तार दोनों ही दृष्टियों से विश्व की अत्यंत प्रतिष्ठित
भाषा है। भाषायी समृद्धि, भौगोलिक विस्तार सास्कृतिक सौंदर्य एवं विश्वदृष्टि आदि आधार पर इसका
राष्ट्रीय एव वैश्विक महत्व है किन्तु दूसरा पहलू यह भी है कि इसके उचित स्थान, सम्मान एव विकास
पर गंभीरतापूर्वक ध्यान की आवश्यकता है। 14 सितम्बर सन 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत यह आवश्यक था कि पूरे देश में इसका समुचित प्रचार-प्रसार हो और पूरे देशवासियों को यह एकसूत्र में पिरो सके। इस उद्देश्य के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदी को विस्तार देने हेतु कई सस्था, संगठन कार्य कर रहे थे। इन्हीं में से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद भारतवासी 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं।
हिंदी मातृभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा आदि विभिन्न रूपों में प्रतिष्ठित है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद क्रमांक 343 से 351 के अंतर्गत इसके राजभाषा संबंधी विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यह उत्तर भारत की मातृभाषा सहित अधिसंख्य भारतवासियों की संपर्क भाषा भी है। आजादी के दौरान सपूर्ण भारतवर्ष को एक उद्देश्य के साथ जोड़ पाने की दृष्टि से सपर्क भाषा की सशक्त भूमिका निभाने वाली इसकी महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने इसे राष्ट्रभाषा कहा था। हालाकि अभी तक इसका कोई सावैधानिक प्रावधान नहीं है किन्तु ध्यातव्य है कि राजभाषा का आधार राज्याश्रय होता है और राष्ट्रभाषा का लोकाश्रय। बहु भाषा भाषी भारतवर्ष में प्रयोक्ताओं को सर्वाधिक संख्या हिंदी भाषा में ही है। इसलिए सर्वाधिक लोकप्रिय और अधिकतर जनमानस की भाषा होने के कारण यह राष्ट्रभाषा के रूप में सर्वस्वीकृति की अधिकारिणी है।
हिन्दी की वर्तमान स्थिति-
हिंदी विशेषज्ञों द्वारा सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि प्रयोक्ताओं की संख्या के आधार पर विश्व में हिंदी की स्थिति तीसरी है और भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से दूसरी। इस संदर्भ में डॉ जयंती प्रसाद नौटियाल द्वारा किए गए शोध अध्ययन 2015 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में हिंदी के प्रयोक्ताओं की सख्या सर्वाधिक 1300 मिलियन है, 1100 मिलियन प्रयोक्ताओं के साथ चीनी द्वितीय स्थान पर तथा 1000 मिलियन प्रयोक्ताओं वाली अग्रेजी तृतीय स्थान पर है। इसी की अगली कड़ी के रूप में 21 अगस्त 2021 को नीदरलैंड में ‘साझा संसार के तत्वावधान में आयोजित वैश्विक सेमिनार आयोजन के दौरान यह बताया गया है कि डॉ नौटियाल द्वारा 2021 भाषा शोध अध्ययन के अनुसार विश्व में हिंदी जानने वालों की संख्या 1356 मिलियन, अंग्रेजी के प्रयोक्ताओं की संख्या 1268 मिलियन और मंदारिन या चीनी के प्रयोक्ताओं की संख्या 1120 मिलियन है। अर्थात् प्रथम स्थान पर हिंदी, द्वितीय स्थान पर अंग्रेजी और तृतीय स्थान पर मदारिन भाषा है। उन्हीं तीनों भाषाओं के मध्य बरसों से सर्वाधिक जनाधार वाली भाषा पर तुलनात्मक चर्चा जारी है। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा बनाए जाने हेतु पहल की गई है किंतु अभी यह कार्य लंबित है। जिन भाषाओं 6 भाषाओं चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश और अरबी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं के रूप में स्वीकृत किए जाने के पीछे यह तर्क था कि इनका भौगोलिक विस्तार विश्व का लगभग आधा भाग है तथा विश्व की आधी आबादी इसकी प्रयोक्ता है। इन भाषाओं की तुलना में हिंदी को देखें तो यह प्रथम स्थान पर है। डॉ. नौटियाल द्वारा किए गए शोध अध्ययन 2015 के अनुसार प्रस्तुत अनुमानित आकड़ों के आधार पर हिंदी के प्रयोक्ताओं की संख्या 1300 मिलियन, चीनी के 1100 मिलियन, अंग्रेजी के 1000 मिलियन, अरबी 460 मिलियन, स्पेनिश 395मिलियन, रूसी 260 मिलियन और फ्रेंच भाषा भाषियों की संख्या 130 मिलियन है। इस प्रकार हिंदी विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा है।

सांस्कृतिक महत्व –
किसी भी भाषा का सबंध अपने नागरिकों के रहन-सहन, आचार-विचार और सम्पूर्ण सास्कृतिक
तत्वों के संवहन से होता है। हिंदी की सास्कृतिक सवहनशीलता का जहाँ तक प्रश्न है, यह बात स्पष्ट
है कि हिंदी भाषा की उम्र लगभग 1000 साल की है किंतु इसके पीछे संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रश,
इत्यादि आर्य भाषा परिवार की कई भाषाओं की उपस्थिति है और इनमें विद्यमान सांस्कृतिक तत्वों की
उपस्थिति कही न कही हिदी में हस्तांतरित हुई है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादि पौराणिक
ग्रंथों में स्थापित मूल्यों, विषयों की उपस्थित हिदी साहित्य के अंतर्गत देखा जा सकता है। अर्थात हजारों
साल का भारतीय साहित्य एवं समाज हिंदी भाषा के अंतर्गत विद्यमान है। उसका संरक्षण संवहन पीढ़ी
दर पीढी निरंतर प्रवाहमान है। हमें अपने समाज के विकास की दृष्टि से धर्म और विज्ञान, साहित्य और
संविधान, कानून और जनरीतियाँ इत्यादि सामाजिक नियत्रण के विभिन्न साधनों को कहीं न कहीं एक
दूसरे से जोडकर चलना होगा। ज्ञान्, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वर्तमान प्रोन्नत युग में भी जिस तरह से
मनुष्यता का स्तर गिरता नजर आता है. वह चिता का विषय है। साहित्य के अंतर्गत विद्यमान जीवन मूल्य
समाज और मानवता को संरक्षित सर्वर्द्धित कर सकते हैं। इस दृष्टि से हिंदी भाषा, साहित्य एवं उनमें
अतर्निहित सांस्कृतिक तत्वों का महत्व असदिग्ध है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा बनना अपेक्षित-
ऊपर जिन तथ्यों के सहारे सयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषाओं की तुलना में हिन्दी के प्रयोक्ताओं की संख्या और भौगोलिक विस्तार को सर्वाधिक माना गया है उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिदी को सयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा के रूप में मान्यता मिलती है तो विश्व की आधी से अधिक लगभग 65 प्रतिशत आबादी और भूभाग संयुक्त राष्ट्र संघ की सात भाषाओं के भीतर स्थान ग्रहण कर सकते हैं और संघ के शक्ति संवर्धन में हिंदी की महती भूमिका सिद्ध हो सकती है यह भारतवर्ष एवं विश्व
समुदाय दोनों के लिए ही कल्याणकारी एवं शुभ सिद्ध होगा।
हिन्दी के समक्ष वर्तमान चुनौतियां एवं अवसर-
अग्रेजी रुझान प्रदर्शित करने वाले लोगों की भी समाज में कमी नहीं है। ये विभिन्न संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों में दृष्टिगोचर होते है और भावी पीढी के समक्ष अंग्रेजी आकर्षण का वातावरण प्रस्तुत करते हैं। देश के भीतर अधिकतर निजी स्कूल बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान कर रहे है। इससे अपनी भाषा में विद्यमान मूल्य चेतना की उपेक्षा होती है। इसी तरह शिक्षित अभिजात्य वर्ग द्वारा विभिन्न मचो पर हिंदी के प्रयोग में हिचकिचाहट और अंग्रेजी बोलने में गौरव महसूस किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। 2011 की जनगणना यह बताती है कि देश की 41 प्रतिशत आबादी हिंदी की प्रयोक्ता है और 75 प्रतिशत भारतीयों की यह दूसरी भाषा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात शिक्षा क्षेत्र से है। देश में उच्च शिक्षा विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा की भाषा अंग्रेजी है। ये सब गभीर विचार-विमर्श के विषय बनते जा रहे है।
अवसर की बात करें तो शिक्षा, शासन-प्रशासन, उद्योग, व्यापार, मनोरजन आदि क्षेत्रों में हिन्दी एक अत्यत समर्थ व उपयोगी भाषा है। तकनीकी दृष्टि से यह निरंतर अद्यतन हो रही है। टकण सुविधाओं का उन्नयन टाइपराइटर और कंप्यूटर के कीपैड से होते हुए अब वॉइस टाइपिंग के रूप में हो चुका है। यूनिकोड जैसी तकनीक के विकास से किसी भी फांट में टंकित सामग्री को किसी दूसरे फाट में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। निरंतर बढ़ती हुई सुविधिाएँ और कार्य करने के आसान तरीके निश्चय ही हिंदी को अत्यधिक युगानुकूल और प्रासंगिक बनाते है। मनोरंजन की दृष्टि से देखें तो हिंदी के गीत सगीत. फिल्म, वेब सीरीज, हारय कार्यक्रम इत्यादि विश्व के कई देशों में मशहूर है। इसी तरह व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से भारत आज विश्व समुदाय के लिए एक बड़ा अवसर प्रदाता देश है। यहाँ विदेशी निवेश बढ़ रहे है और उद्योग धंधों का विकास भी हो रहा है। इस तरह की अनेक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान युग में हिन्दी भाषा के आगे चुनौतियों के साथ-साथ अनेक अवसरों के मार्ग भी प्रशस्त हुए है।
हिन्दी का भविष्य और भविष्य की हिन्दी-
उपर्युक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए लगता है कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है। आने वाले समय में निश्चित रूप से यह भारतवर्ष में पूर्ण प्रसार के साथ-साथ विश्व स्तर पर भी मजबूत उपस्थिति की ओर अग्रसर है। इसकी विकास यात्रा से ज्ञात होता है कि जैसे-जैसे तकनीक का विकास हुआ. व्यापार में वृद्धि हुई विश्व के कई क्षेत्रों से लोग हिंदी भाषा के संपर्क में आए और जो जहाँ से आए वे अपनी भाषा के कुछ शब्द भी लेकर आए साथ ही अपने सस्कृतिक तत्व भी। धीरे-धीरे हिंदी का इसी तरह विकास हुआ। दिन प्रतिदिन उसकी समाहार शक्ति बढ़ती गई। साहित्य की दृष्टि से देखे हैं तो रूस. फ्रांस इत्यादि विभिन्न देशों से विधेयवाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद, विखडन इत्यादि वैचारिक पृष्ठभूमि के तत्व आए। इन सब ने भारतीय वैचारिकी के साथ स्वयं को जोडते हुए आधुनिक हिंदी को शिल्प एवं भाव दोनों ही दृष्टिया से पुष्ट किया, उसका विकास किया। विकास यात्रा जारी है तो निश्चय ही यह मानकर चला जा सकता है कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है और भविष्य की विकसित, बलवती एवं व्यापक हिंदी के द्वारा भारतवर्ष और विश्व के प्रति उसकी भूमिका में भी अभिवृद्धि होगी। वह भारतीय चितन परपरा में प्रकारांतर से विद्यमान विश्व दृष्टि, संपूर्ण समाज की कल्याण कामना व भावना को कहीं न कही गति एवं दिशा देने में अधिक सशक्त उपस्थिति दर्ज करने वाली सिद्ध होगी, ऐसा प्रतीत और विश्वास होता है।
निष्कर्षस्वरूप संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत्तवर्ष ने अपनी आजादी की 100 वी वर्षगांठ अर्थात् सन् 2047 में विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व समुदाय के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करने का जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है उसे पूर्ण करने में भाषा के रूप में हिंदी की विशिष्ट भूमिका सिद्ध होगी। शिक्षा, प्रशासन, उद्योग, व्यापार, मनोरंजन इत्यादि क्षेत्रों में इसकी वैश्विक प्रसिद्धि और सामर्थ्य, प्रयोक्ताओं की विश्व में सर्वाधिक संख्या और भौगोलिक विस्तार आदि विवध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा के रूप में मान्यता मिलने की भी अपेक्षा है। भारत की उदात्त चिंतन परंपरा के सुदीर्घ इतिहास में संचित कला, साहित्य, संस्कृति जीवन मूल्यों एवं सामाजिक आदर्शा का संवहन करने में यह पूर्ण रूपेण अभिव्यक्ति क्षमतायुक्त है। विश्व कल्याण की कामना और भूमिका में भी यह सदैव की तरह आगे भी सहायक सिद्ध होती रहेगी. ऐसा विश्वास है।
हिन्दी दिवस की शुभकामनाएँ,
जय हिन्द, जय हिन्दी।